

16 August 2025

भारत में दो विभाग हैं जो करों का संग्रहण करते हैं। एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, जिसे प्रत्यक्ष कर निदेशालय भी कहते हैं, जिसका जिम्मा आपकी आय/आमदनी पर टैक्स लगाना है।
दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) अप्रत्यक्ष करों—GST (CGST/IGST), कस्टम/सीमा शुल्क—और शेष केंद्रीय उत्पाद शुल्क का प्रशासन करता है; CBIC का पूर्व नाम CBEC (एक्साइज व कस्टम्स) था। CBDT (प्रत्यक्ष कर) और CBIC (अप्रत्यक्ष कर) दो अलग-अलग बोर्ड हैं।
दोनों का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के लिए कर संग्रह करना है। ये दोनों विभाग पिछले 10–11 वर्षों से जनता के हित में अच्छे निर्णय ले रहे हैं। भारत का जो कर संग्रह का मॉडल पिछले 10–11 वर्षों से चल रहा है, उसे विश्व के बाकी देशों को भी समझना चाहिए कि हमारी वर्तमान सरकार करों का संग्रह कितनी खूबसूरती से कर रही है।
टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम/सीमा शुल्क और एंटी-डंपिंग ड्यूटी क्या हैं?
जब से इस वर्ष जनवरी में अमेरिका में ट्रंप सरकार आई, तब से “टैरिफ” शब्द की खूब चर्चा हो रही है और साथ में जुड़ गया है एक अनोखा शब्द “वॉर” तो कुल मिलकर एक नया शब्द हो गयाहै “टैरिफ वॉर” —यह क्या है, इसके मायने क्या हैं, किसको ज्यादा नुकसान होगा और किसको कम फायदा—यह समझना हर नागरिक के लिए जरूरी है। जब भी कोई देश किसी अन्य देश से आयात करता है, तो उस पर सीमा शुल्क/कस्टम ड्यूटी लगती है। कस्टम ड्यूटी लगाने का मूल उद्देश्य यह है कि आयात पर वाजिब शुल्क लगे, अप्रत्यक्ष कर और कर संग्रह में वृद्धि हो—राष्ट्र निर्माण के लिए यही मूल मंत्र है। अब सवाल आता है कि इसकी दरें कितनी हों।
जो देश आयात करता है, वह पहले जांचता है कि किसी वस्तु का घरेलू उत्पादन आवश्यकता से कम है या ज्यादा। यदि उत्पादन कम और जरूरत ज्यादा है, तो सीमा शुल्क वाजिब तरीके से लगाया जाएगा, ताकि देश के उत्पादकों और आयातकों—दोनों—को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, नागरिकों पर अनावश्यक कर बोझ न पड़े, और दामों में अत्यधिक अंतर से प्रतिस्पर्धा-विकृति न हो। अत्यधिक अंतर और गैर-जरूरी प्रतिस्पर्धा गलत प्रैक्टिस मानी जाती है।
एंटी-डंपिंग ड्यूटी का अर्थ है: यदि किसी देश में उसके उत्पादक अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन कर रहे हैं और घरेलू मांग पूरी कर पा रहे हैं, फिर भी कोई दूसरा देश अपने निर्यातकों को सब्सिडी/छूट देकर दूसरे देश के उद्योगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो आयातक देश अपने उत्पादकों की सुरक्षा हेतु आयातित माल पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाता है, ताकि कोई देश अपना अतिरिक्त उत्पादन दूसरे देश में डंप न कर दे। इसका उद्देश्य अपने देश के उत्पादन और उद्योगों को संरक्षण देना है। कई बार सैन्य कार्रवाई संभव न होने पर देश आर्थिक युद्ध छेड़ देते हैं, जिससे विरोधी देश की औद्योगिक क्षमता और व्यापार चक्र बाधित हो। इसी जोखिम से बचाव के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है।
सरकार एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी ड्रॉ-बैक का लाभ भी देती है। यदि निर्माण लागत अधिक होने से निर्यातक प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हों, तो निर्यात मूल्य पर 2% से 25% तक का ड्यूटी ड्रॉ-बैक दिया जा सकता है। उदाहरण: किसी कंपनी ने 1 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है और किसी विशेष देश के लिए 20% ड्यूटी ड्रॉ-बैक घोषित है, तो सरकार 20% यानी 20 लाख डॉलर का क्रेडिट निर्यातक को देती है। उद्देश्य है: निर्यात, रोजगार, औद्योगिक क्षमता, व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। इसमें विस्तृत गणना और सिस्टम होते हैं; सामान्यतः मनमानी नहीं की जा सकती, और सरकारें इसे पारदर्शिता से लागू करने का प्रयास करती हैं—जब तक कि कोई विशेष देश बदले की भावना से कार्रवाई न करे।
भारत में भी 2000 से पहले तक निर्यात पर आयकर में विभिन्न रूपों में छूट मिलती थी—कभी पूरी छूट, कभी स्लैब/धाराओं में बदलाव—ताकि भारतीय उद्योगपति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहें, रोजगार और औद्योगिकीकरण बढ़े, और भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हो। इसी उद्देश्य से आयकर छूट/ड्यूटी ड्रॉबैक जैसे प्रावधान रहे।
अब ट्रंप सरकार और टैरिफ वॉर पर आते हैं। मेरे मत में या तो सलाहकार पारदर्शिता से काम नहीं कर पा रहे, या नेतृत्व स्वार्थवश बिना ठोस आधार के अलग-अलग देशों/सामानों पर आयात दरें मनमाने तरीके से तय कर रहा है। उदाहरण: यदि अमेरिका किसी विशेष आइटम पर 50% टैरिफ लगा दे—मान लें पहले 100,000 डॉलर के आयात पर 20% ड्यूटी लगती थी, तो लैंडेड कीमत 120,000 डॉलर होती थी; 50% टैरिफ होने पर यह 150,000 डॉलर हो जाएगी। प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज, विज्ञापन, मटेरियल मैनेजमेंट, हैंडलिंग, सप्लाई चेन आदि के खर्च भी अनुपातिक रूप से बढ़ेंगे। यानी लैंडिंग कॉस्ट पर ही 25–30% बढ़त, और आगे उपभोक्ता तक डिलीवरी तक अतिरिक्त लागत। पहले जहां 120,000 डॉलर की लैंडेड कॉस्ट पर वस्तु लगभग 200,000 डॉलर में बिकती थी, अब 150,000 डॉलर की लैंडेड कॉस्ट पर यह 225,000–250,000 डॉलर तक जा सकती है। क्योंकि 20% की जगह 50% ड्यूटी से ड्यूटी, ब्याज, डेप्रिसिएशन और अन्य प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष खर्च अनुपात में बढ़ते हैं।
अंततः नुकसान आयातकर्ता देश के उपभोक्ता/नागरिक का है जिसे पहले 200,000 डॉलर में मिलने वाली वस्तु अब 250,000 डॉलर तक मिलेगी। नतीजा: आयातक देश में महंगाई, संभावित बेरोजगारी, और सामाजिक-आर्थिक तनाव। शुरुआती चरण में सरकार को टैरिफ से राजस्व मिल सकता है, पर अंततः उपभोक्ता-पीड़ा और अर्थव्यवस्था पर असर से नुकसान की भरपाई कठिन हो जाती है।
सरकार का काम कर लगाना है, पर चाणक्य नीति कहती है: कर उतना ही जैसे आटे में नमक—ज्यादा होगा तो स्वाद खराब, कम होगा तो स्वादहीन। इसलिए, संयुक्त राष्ट्र के लगभग 198 देशों की सरकारों से—मैं एक लेखक और अपने 45 वर्षों के व्यापारिक अनुभव के आधार पर—निवेदन करता हूँ कि करारोपण से पहले देखें कि दोनों पक्षों में किसे कितना लाभ/हानि होगी। मैंने बजट से पहले कई बार वित्त मंत्रालय को सुझाव भेजे हैं: जब भी सिक्योरिटीज ट्रांज़ैक्शन टैक्स (एसटीटी), लॉन्ग-टर्म/शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन की अवधियां/दरें बदली जातीं और 2–3 हजार करोड़ अतिरिक्त वसूली का अनुमान लगाया जाता, बाजार तुरंत नकारात्मक प्रतिक्रिया देता। कई बार दिन के अंत तक 20–30 हजार करोड़, और कभी-कभी 2–3 लाख करोड़ रुपए तक का मार्केट कैप घट जाता है , लाखों निवेशकों का पैसा फंसता, और लोग बाजार से बाहर हो जाते।
अतः मेरी सभी सरकारों से प्रार्थना है: नागरिकों को खुश रखना आपका काम है। कर लगाने की मंशा बनाते समय गहरा होमवर्क करें—लगाने/न लगाने से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नफा-नुकसान क्या होंगे, जनता में कैसा परसेप्शन बनेगा, विपक्ष क्या नैरेटिव खड़ा करेगा। आज सोशल मीडिया के दौर में परसेप्शन और नैरेटिव से सरकारें बदल जाती हैं। इसलिए टैक्स लगाने से पहले बाजार विशेषज्ञों से सलाह लें—निगेटिव/पॉजिटिव इम्पैक्ट कितने होंगे—और समझ आने पर ही घोषणा करें। फिर प्रेस ब्रीफिंग में साफ बताएं कि कर क्यों लगाया, क्या मंशा थी, दीर्घकाल में जनता, देश और राष्ट्र निर्माण के लिए विजन क्या है; और यह राजस्व किन क्षेत्रों में, कैसे, और किन अपेक्षित अच्छे परिणामों के लिए खर्च होगा। जनता को यह समझाना भी सरकार की जिम्मेदारी है।
आशा है, आप इसे साझा करेंगे और जनमानस को जागरूक करेंगे, क्योंकि आज के समय में फाइनेंस समझना हर व्यक्ति के उज्ज्वल भविष्य के लिए जरूरी है। चाहे आप विज्ञान, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या शिक्षण के पेशे में हों—अंततः आपका जीवन आपकी आय पर ही चलता है; इसलिए फाइनेंस की बुनियादी जानकारी आवश्यक है। मेरा यह लिखने का उद्देश्य भी यही था।
मेरा सभी सरकारों से पुनः निवेदन है कि इन सुझावों को सकारात्मक रूप में लें। जब भी टैक्स का करारोपण करें—भारत हो या अन्य देश—इन बातों पर ध्यान दें, अनावश्यक विवादों से बचें और विश्व में शांति का वातावरण बनाएं। एक-दूसरे को नीचा दिखाना/डुबोना और उद्योग-धंधे बर्बाद करना सरकारों का काम नहीं है। सरकारों का काम है प्रजा को खुश, संपन्न, प्रभावशाली और खुशहाल बनाना; रोजगार के अवसर बढ़ाना; अराजकता से बचाना। ऐसा कोई कानून/करारोपण न हो जिससे असमंजस या अव्यवस्था पैदा हो। राष्ट्र निर्माण के लिए कर निर्धारण करने वालों—सरकारी अधिकारियों और नीति-निर्माताओं—को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा न हो की यह कहावत सही में चरितार्थ हो जाये कि “अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत”।
रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड।
जयपुर, राजस्थान
suneelduttgoyal@gmail.com
Blogs/Topics


















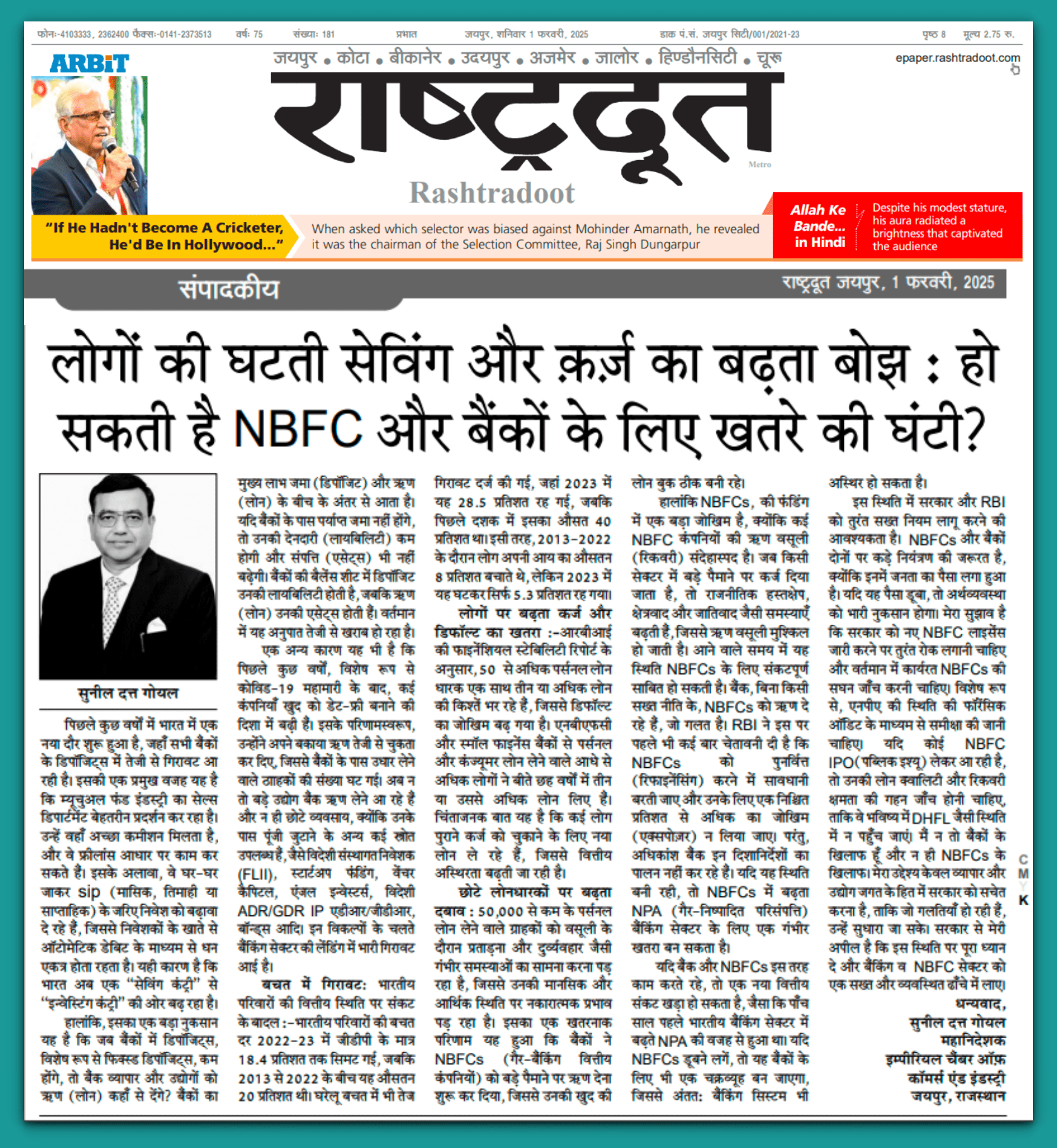














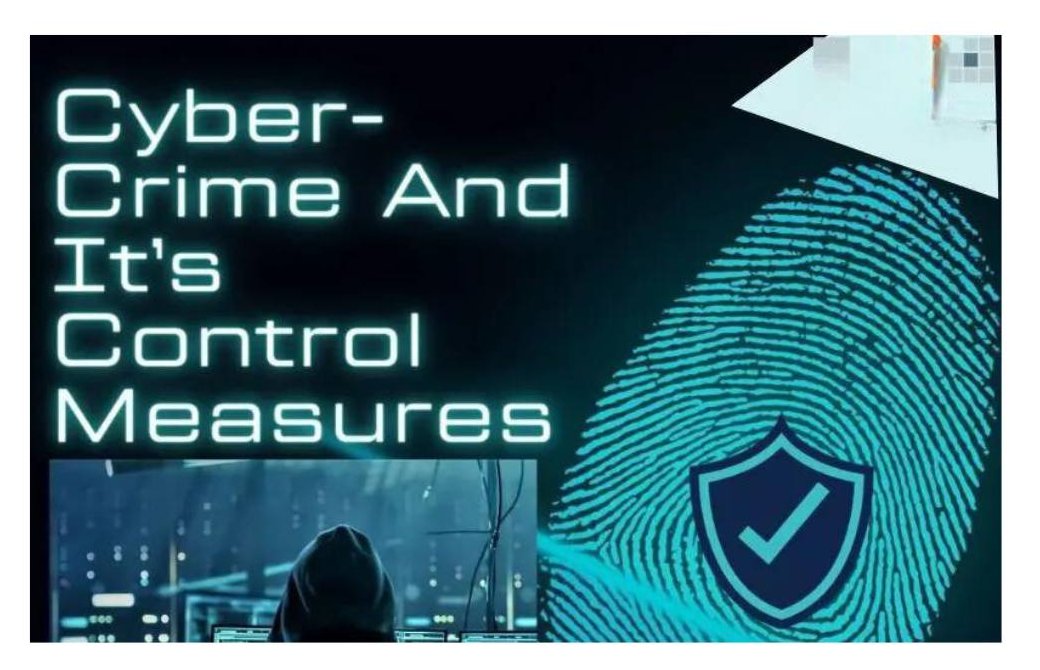







Rtn. Suneel Dutt Goyal